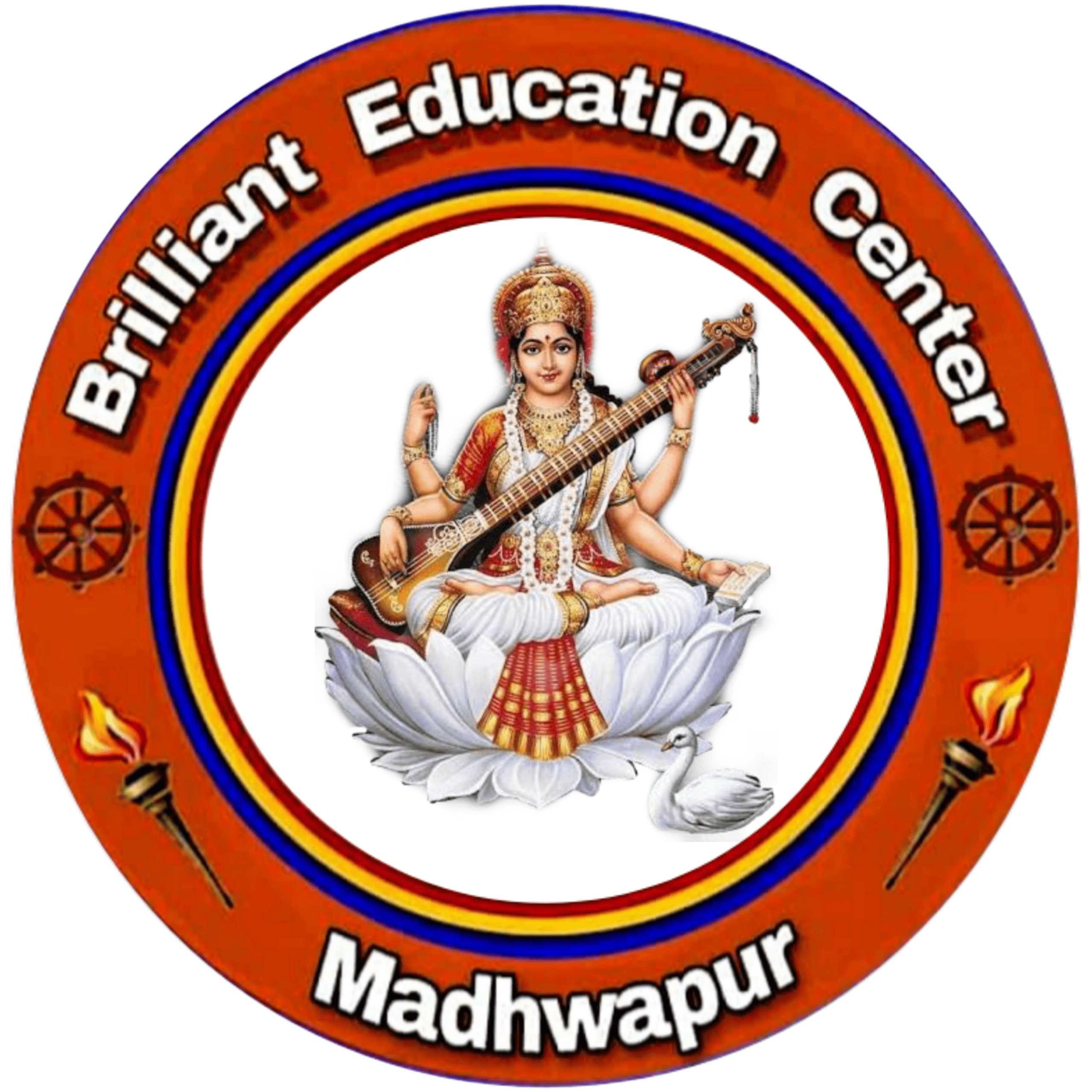विद्यापति के पद (vidyapati ke pad)
vidyapati ke pad
प्रश्न 1.
राधा को चन्दन भी विषम क्यों महसूस होता है?
उत्तर-
मैथिल कोकिल विद्यापति विरह-बाला राधा की विरह वेदना का चित्रण करते हुए कहते हैं कि सपना में भी श्रीकृष्ण का दर्शन नहीं होता है। श्रीकृष्ण का दर्शन नहीं होने से राधा का हृदय आतुर और व्याकुल है। इस विरह-वेदना में चन्दन जो शीतल और आनन्ददायक है वह भी विष के समान होकर उसके शरीर को तीष्ण और उष्ण कर रहा है। विरह-वेदना ने उसकी मानसिक पीड़ा को बढ़ा दिया है।
प्रश्न 2.
राधा की साड़ी मलिन हो गयी है। यह स्थिति कैसे उत्पन्न हो गयी?
उत्तर-
कृष्ण-सखा उद्धव के कहे अनुसार मथुरा से कृष्ण आने वाले हैं। अतः राधा श्रृंगार कर नयी साड़ी पहन कर कृष्ण के आने की बाट जोह रही है किन्तु विरह की अवधि जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, राधा की बेचैनी और बढ़ती जाती है। वह धीरे-धीरे विस्तृति की अवस्था को प्राप्त हो जाती है। उसे अपने शरीर की सुध-बुध भी नहीं रहती। फलतः उसकी साड़ी रास्ते की धूल, हवा, पानी आदि के प्रभाव से मलिन हो जाती है, गन्दी हो जाती है।
प्रश्न 3.
“चन्द्रबदनि नहि जीउति रे, बध लागत काहे।” इस पंक्ति,का क्या आशय है?
उत्तर-
प्रस्तुत पंक्ति मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा विरचित पद-1 से ली गई है। कवि ने श्रीकृष्ण के विरह में राधा की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया। मैथिल कोकिल विद्यापति ने राधा के विरह की उत्कट व्यंजना की है। श्रीकृष्ण के गोकुल आने के इन्तजार में राधा को चन्दन भी विष के समान प्रतीत होता है। शरीर पर किए गए गहने से उसे भारी पड़ रहे हैं। इसका कारण श्रीकृष्ण के साक्षात् दर्शन की बात तो दूर है, वह सपने में भी उसे दिखाई नहीं देते हैं। उनके आने के इन्तजार में विरह-बाला राधा कदम्ब के पेड़ के नीचे अकेली खड़ी है। उसकी साड़ी का रंग मलिन को रहा है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा
vidyapati ke pad
प्रश्न 4.
विद्यापति विरहिणी नायिका से क्या कहते हैं? उनके कथन का क्या महत्त्व है?
उत्तर-
शृंगार रस के सिद्धहस्त कवि विद्यापति के अनुसार राधा कृष्ण-विरह की अग्नि में दग्ध होती, राधा जो अपनी सुध-बुध खो चुकी है, निराश हो चुकी है। विरह की दस दशाओं में अन्तिम दशा मरण को प्राप्त सी हो गयी है। ऐसी परिस्थिति में उसके भीतर आशा का, जीवन का संचार करने के उद्देश्य से विद्यापति कहते हैं कि आज कृष्ण गोकुल आने वाले हैं। ऐसी सूचना मिली है कि कृष्ण मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अतः तुम शीघ्रता से कृष्ण मग में जाकर उनकी प्रतीक्षा करो। कहीं मिलन, संयोग की यह अनुपम, विलक्षण घड़ी से तुम वंचित न रह जाओ।
प्रश्न 5.
प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें।
उत्तर-
प्रश्न 6.
नायिका के मुख की उपमा विद्यापति ने किस उपमान से दी है। प्रयुक्त उपमान से विद्यापति क्यों संतुष्ट नहीं हैं?
उत्तर-
महाकवि विद्यापति ने “सरस बसंत समय भल पाओल” में नायिका राधा के शरीर (मुख) की उपमा देने के लिए चन्द्रमा जैसे विश्व प्रसिद्ध उपमान का प्रयोग किया है। किन्तु अपने ही प्रयुक्त उपमान से कवि संतुष्ट नहीं है। इसका कारण है कि चन्द्र की नित्य प्रति बदलने वाली स्थिति। विधि, विधाता ने अनेक बार इस चन्द्र में काट-छाट की। इसे बढ़ाया, घटाया फिर भी यह वह योग्यता नहीं प्राप्त कर सका कि विद्यापति की नायिका के शरीर के लिए उपमान – बन सके। वस्तुतः विद्यापति की नायिका “श्यामा” नायिका है, जिसका सौन्दर्य लावण्य “तिल-तिल, नूतन होय” वाला है। अतः उसके आगे चन्द्रमा जैसा उपमान भी कैसे टिक सकता है।
vidyapati ke pad
प्रश्न 7.
कमल आँखों के समान क्यों नहीं हो सकता? कविता के आधार पर बताएँ। आँखों के लिए आप कौन-कौन सी उपमाएँ देंगे। अपनी उपमाओं से आँखों का गुण साम्य भी दर्शाएँ।
उत्तर-
महाकवि विद्यापति ने “सरस बसंत समय भल पाओल” पद में नायिका के रूप में सौन्दर्य का वर्णन करते हुए उसकी आँखों के लिए कमल की उपमा दी है। किन्तु अगली ही पंक्ति में इस उपमान को वे समीचीन मानने से अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि कमल का जीवन क्षणिक है। साथ ही सूर्य के उदीयमान अवस्था में ही वह प्रस्फुटित होता है। रात्रि में उसकी पंखुड़ियाँ बंद हो जाती हैं।
प्रश्न 8.
निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य-सौन्दर्य स्पष्ट करें:
(क) भनई विद्यापति मन दए रे, सुनु गुनमति नारी,
आज आओत हरी गोकुल रे, पथ चलु झट-झारी।
उत्तर-
प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव एवं नवकवि शेखर जैसी उपाधियों से विभूषित महाकवि विद्यापति के पद से उद्धृत हैं। इसमें कवि ने वीर-विदग्धा नायिका को प्रबोध दिया है। वे कहते हैं कि हे गुणवती नारी (राधा)! तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनो। आज हरि (श्रीकृष्ण) गोकुल से आने वाले हैं। इसलिए तुम झटपट उनसे मिलने के लिए चल पड़ो।
vidyapati ke pad
(ख) लोचन-तूल कमल नहिं भए सक, से जग के नहिं जाने।
से फेरि जाए नुकाएल जल भए, पंकज निज अपमाने ॥
उत्तर-
प्रस्तुत पंक्तियाँ हिन्दी के अमर महाकवि विद्यापति के पद से अवतरित हैं। इस पद में कवि ने नायिका के सौंदर्य के सामने कवि-जगत में प्रसिद्ध सुंदरता के प्रसिद्ध उपमानों को फीका दिखाया है। यहाँ कवि ने कहा है कि कमल, जो सुंदरता के लिए जाना जाता है, वह भी तेरे नेत्रों की सुंदरता की समानता न कर सका, कदाचित इसी अपमान और लज्जा के कारण वह जग की आँखों से दूर जल में छिप गया है।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना-शक्ति का चमत्कार देखते ही बनता है। कमल को नायिका के नेत्रों में हीनतर सिद्ध किया गया है। अतः इसका काव्य-सौंदर्य सर्वथा सराहनीय है।
प्रश्न 9.
द्वितीय पद (सरस बसंत समय भल पाओल) का भावार्थ प्रस्तुत करें।
उत्तर-
एक ही वर्ण की अनेकशः आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं।
यहाँ “भूषण भेल भारी” में ‘भ’ वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह देह-दग्ध, जाह जाह……….मधु पुर जाहे आज आओत और झट-झारी में अनुप्रास अलंकार है।
प्रश्न 2.
चन्द्रवदनी में रूपक अलंकार है। रूपक और उपमा में क्या अंतर है? उदाहरण के साथ स्पष्ट करें।
उत्तर-
जहाँ दो भिन्न पदार्थों के बीच सादृश्य या साधर्म्य की स्थापना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। किसी भी वस्तु के विषय में अपनी भावना का अधिक सबलता सुन्दरता और स्पष्टता से अभिव्यक्त करने के लिए हम किसी दूसरी वस्तु से जिसकी वह विशेषता ख्यात हो उसका सादृश्य दिखाते हैं।
उपमा में चार तत्त्व होते हैं-
(क) उपमेय,
(ख) उपमान,
(ग) साधारण धर्म तथा
(घ) वाचक।
vidyapati ke pad
प्रश्न 3.
दूसरे पद में कवि ने नायिका के सौन्दर्य के लिए कई उपमाएँ दी हैं। प्रयुक्त उपमेयं की उपमानों के साथ सूची बनाएँ।
उत्तर-
विद्यापति रचित पद ‘सरस बसंत समय भल पाओल’ में नायिका राधा के लिए निम्नलिखित उपमान प्रयुक्त किये गये हैं।
उपमेय – उपमान
बदन (मुख) – चन्द्रमा (चान)
लोचन (नयन) – कमल
प्रश्न 4.
निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें हरि, देह, चन्द्रमा, पथ, पवन, कमल, लोचन, जल।
उत्तर-
हरि-विष्णु, देह-शरीर, चन्द्रमा-निशाकर, पथ-रास्ता, पवन-हवा, कमल-पंकज, लोचन-आँख, जल-पानी। .
vidyapati ke pad
प्रश्न 5.
निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखें दगध, भूषन, गुनमति, दछिन, पवन, जौबति, बचन, लछमी।
उत्तर-
दगध-दग्ध, भूषण-भूषण, जनमति-गुणमति, दछिन-दक्षिण,
पबन पवन, यौवति-युवति, वचन-वचन, लक्ष्मी-लक्ष्मी।
vidyapati ke pad
प्रश्न 6.
दोनों पदों में प्रयुक्त मैथिली शब्दों की सूची तैयार करें और उनके संगीत अर्थ एवं रूप स्पष्ट करें तथा वाक्यों में प्रयोग करें। .
उत्तर-
चानन (चंदन) – चंदन शीतलता देता है।
‘सर (सिर, माथा) – उसका सिर भारी है।
भूषण (गहना) – आभूषण कीमती है।
भारी (भारस्वरूप) – यह भारी जवाबदेही है।
एकसरि (अकेला) – वह अकेला इस सम्पत्ति का स्वामी है।
पथ हेरथि (रास्ता देख रही है) – विरहिणी प्रेम का रास्ता देख रही है।
दगध (दग्ध) – मेरा हृदय विरह ज्वाला से दग्ध है।
झामर (मलिन) – गर्मी से चेहरा मलिन हो गया है।
जाह (जाओ) – अब तुम यहाँ से चले जाओ।
जीउति (जीवित रहेगी) – पानी बिना मछली कब तक जीवित रहेगी।
बध (वध) – किसी का भी वध करना पाप है।
काहे (क्यों) – तुम यह बात क्यों पूछ रहे हो?
झटझारी (झटक कर) – गाड़ी पकड़नी है तो झटक कर चलो।
- vidyapati ke pad
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
विद्यापति की सौन्दर्य-दृष्टि पर प्रकाश डालें।
उत्तर-
विद्यापति की दृष्टि में सौन्दर्य नित नूतन होता है। वह किसी भी लौकिक उपमान से तुलनीय नहीं होता। अपनी नायिका की उपमा हेतु चाँद और कमल को अयोग्य मानकर कवि ने इस तथ्य को व्यक्त किया है। कवि ने सुन्दर नारी को लक्ष्मी के समान कहा है। अत: उसके अनुसार सौन्दर्य ऐश्वर्यपूर्ण कल्याणप्रद होता है।
vidyapati ke pad
प्रश्न 2.
राधा के मरने का पाप किसे लगेगा?
उत्तर-
राधा विरह का दंश झेल रही है। अतः उसके मरने का पाप कृष्ण को लगेगा। उद्धव समाचार लेने आये हैं। यदि वे जाकर राधा की दशा कृष्ण को नहीं बतायेंगे तो राधा के मरने का पाप उन्हें ही लगेगा। अत: उद्धव राधा की हालत को कृष्ण को बताने के लिए व्यग्र हो जाते
प्रश्न 3.
कमल जल में जाकर क्यों छिप गया है?
उत्तर-
विद्यापति की दृष्टि में कमल को नायिका के मुख की समानता करने लायक या उपमान बनने लायक क्षमता नहीं प्राप्त है। अतः वह अपने अपमान के कारण जल में जाकर छिप गया है। वास्तव में, कमल जल में ही खिलता और पनपता है।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1.
राधा कदम्ब के नीचे क्या कर रही है?
उत्तर-
राधा विरह में व्याकुल खड़ी है। वह कदम्ब के नीचे अकेले खड़ी होकर कृष्ण के मथुरा से गोकुल लौटने की प्रतीक्ष कर रही है।
प्रश्न 2.
कृष्ण के बिना राधा की दशा कैसी है?
उत्तर-
कृष्ण के बिना राधा का हृदय दग्ध हो रहा है। उसे भूषण भार स्वरूप प्रतीत हो रहे हैं तथा शरीर पर लगा चन्दन का प्रलेप तीक्ष्ण बाणों की तरह चुभ रहा है।
प्रश्न 3.
विद्यापति गोपियों और राधा को क्या आश्वासन देते हैं?
उत्तर-
विद्यापति आश्वासन देते हैं कि कृष्ण आज गोकुल वापस लौटेंगे। अतः तुम लोग शीघ्र गोकुल लौट जाओ।
प्रश्न 4.
चाँद नायिका के मुख के समान क्यों सुन्दर नहीं है?
उत्तर-
चाँद को कई बार काट-छाँट कर विधाता ने अधिक-से-अधिक सुन्दर बनाने का प्रयास किया है लेकिन वह नायिका के सौन्दर्य की तरह नित-नूतनता धारण नहीं कर पाया है।
प्रश्न 5.
स्वप्न पुरुष नायिका के मुख से चीर हटाने के लिए क्यों कहता है?
उत्तर-
स्वप्न पुरुष नायिका का रूप देखना चाहते हैं। वस्तुत: नायिका अवगुंठन में है। अतः विद्यापति स्वयं उसका सौन्दर्य देखने हेतु स्वप्न पुरुष के बहाने की उसकी प्रशंसा कर रहे हैं।
vidyapati ke padप्रश्न 6.
विद्यापति की दृष्टि में सौन्दर्य कैसा होता है?
उत्तर-
विद्यापति की दृष्टि में सौन्दर्य अनुपम होता है जो लक्ष्मी की तरह ऐवW, शोभ और मंगल से युक्त होने के कारण त्रिवेदी होता है। वस्तुतः सुन्दरता गुण में परिलक्षित होता है।
प्रश्न 7.
विद्यापति के प्रथम पद में श्रृंगार के किस पक्ष को उद्घाटित किया गया है?
उत्तर-
विद्यापति के प्रथम पद में श्रृंगार के वियोग पक्ष को उद्घाटित किया गया है।
प्रश्न 8.
विद्यापति ने मूख की तुलना किससे की है?
उत्तर-
विद्यापति ने मुख की तुलना चन्द्रमा से की है।
1. चानन भेल विषय सर…………….गिरधारी।
व्याख्या-
प्रस्तुत पद विद्यापति द्वारा रचित है। पूरे पद के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यह गोपी-उद्धसंवाद के रूप में रचित है। इसके अनुसार उद्धव की जिज्ञासा के उत्तर में गोपियाँ राधा की विरह-दशा का वर्णन कर रही हैं। वे बताती हैं कि कृष्ण के वियोग में राधा के शरीर में लगा चन्दन-प्रलेप शीतलता प्रदान करने के बदले तीक्ष्ण बाण की तरह चुभ रहा है। शारीरिक दुर्बलता के कारण अथवा प्रसाधनों की नि:सारता अनुभव करने के कारण आभूषण बोझ की तरह लग रहे हैं। पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा करने वाले दयालु कृष्ण अब इतने निष्ठुर हो गये हैं कि राधा को सपने में भी दर्शन नहीं देते। इस तरह वियोग-व्यथिता राधा की दशा अत्यन्त विषम है।
2. एकसरि ठाढ़ि कदम-तरे रे………………..झामर भेल सारी।
व्याख्या-
प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों उद्धव से बता रही हैं कि राधा अकेले कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। कृष्ण के न आने से उत्पन्न निराशा और वियोग के ताप से उनका हृदय दग्ध हो रहा है, जल रहा है। वियोग के कारण श्रृंगार प्रसाधन के प्रति कोई रुचि नहीं है, उत्साह नहीं है। अत: वस्त्र बदलने की भी सुधि नहीं है। फलतः साड़ी झामर अर्थात् मलिन हो गयी है। यहाँ कवि ने राधा के मन की पीड़ा और प्रसाधन के प्रति उत्साह के अभाव को व्यक्त करने का प्रयास किया है। ‘हृदय दग्ध’ और ‘झामर साड़ी’ के द्वारा मन और तन दोनों की वेदना अभिव्यक्त हुई है।
3. जाह जाह तोहें उपव है……………बध लागत काहे।
व्याख्या-
विद्यापति रचित इन पंक्तियों में गोपियों उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव तुम मथुरा लौट जाओ। वहाँ कृष्ण को राधा की दशा बता देना कि चन्द्रमा के समान मुखवाली राधा जीवित नहीं रह पायेगी। यदि उन्हें दया लगेगी तो आकर बचा लेंगे। तब उन्हें राधा के मरने का पाप क्यों लगेगा? दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि तुम मथुरा लौट कर कृष्ण को सारी बातें बात यो। ऐसा करने पर तुम अपने दायित्व का निर्वाह कर लोगे और तुम्हें राधा के मरने का पाप नहीं लगेगा। तब पाप कृष्ण को लगेगा तुम्हें नहीं। यहाँ कवि ने विरह में मरण-दशा का उल्लेख किया है।
4. भनइ विद्यापति मन दए…………..झट-झारी।
व्याख्या-
विद्यापति ने अपने पद की पूर्व पंक्तियों में विरह मरण का वर्णन किया है। यह तत्त्व शृंगार का विरोधी होता है। मरण शोक का विषय है जो वरुण रस का स्थायी भाव होता है। इसका परिमार्जन करने के लिए कवि ने इन पंक्तियों में कृष्ण के आगमन की सूचना देकर आशा का. आलम्बन थमा दिया है।
कवि गोपियों तथा राधा दोनों को सम्बोधित कर कहता है कि हे गुणवती नारियों तन मन देकर अर्थात् ध्यान देकर सुनो। आज कृष्ण मथुरा से गोकुल आवेंगे। अतः तुम पंग झाड़कर अर्थात् शीघ्रता से गोकुल चलो। यहाँ कवि द्वारा एक मनोवैज्ञानिक झटका दिया गया है। कृष्ण के आने की सूचना से राधा के मन की निराश-भाव लगेगा और उसकी मनोदशा बदलेगी। गोपियाँ राधा को लेकर गोकुल लौटेंगी और इस प्रक्रिया में जो परिवर्तन होगा वह विरहिणी को थोड़ी गहत दे सकेगा। अत: इन पंक्तियों में कवि द्वारा आशावाद के सहारे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने की चेष्टा की गयी है।
vidyapati ke pad
5. सरस वसंत समय भल…………….दुरि करु चीरे।
व्याख्या-
महाकवि विद्यापति ने अपने पद की इन पक्तियों में एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया है। पृष्ठभूमि यह है कि बसंत ऋतु का सुन्दर समय आ गया है। दक्षिण पवन बहने लगा है। यह हवा बसंत ऋतु में बहती है और प्रायः दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी गति होती है। यह पवन शील, मन्द और सुखद होता है। इसी भौतिक परिवेश में नायिका सोयी हुई है। उसने सपने में देखा कि कोई सुन्दर पुरुष आकर उससे कह रहा है कि तुमने साड़ी से अपने सुन्दर मुख को क्यों हँक रखा है। मुख पर से चीर हटाओ। अभिप्राय है कि इस सरस मनोरस वासन्ती समय में जब दक्षिण पवन बह रहा है तब सुन्दर मुख को ढकने का नहीं रूप को प्रदर्शित करने का समय है अतः अपना सुन्दर रूप मुझे देखने दो।
vidyapati ke pad
6. तोहर बदन सन चान होअथि…………तुलित नहिं भेला।
व्याख्या-
अपने शृंगारिक पद की इन पंक्तियों में विद्यापति कहते हैं कि उस स्वप्न पुरुष ने उस सुन्दरी नायिका से कहा है कि तुम्हारा रूप अनुपम है। तुम्हारे मुख के समान चाँद भी नहीं है। विधाता ने सुन्दरता के प्रतिमान के रूप में चाँद को कई बार काट-छाँट कर नया बनाया ताकि वह तुम्हारे मुख का उपमान बन सके। लेकिन इतना करने पर भी वह तुम्हारे मुख की उपमा के योग्य नहीं बन सका। यहाँ कविं स्वप्न पुरुष के कथन के माध्यम से नायिका को यह बताना चाहता है कि तुम्हारा मुख चाँद से अधिक सुन्दर है।
7. लोचन-तूल कमल नहि भए सक……………निज अपमाने।
व्याख्या-
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नायिका के नेत्रों की उपमा हेतु कमलों को अयोग्य ठहराते हुए कहता है कि तुम्हारे नेत्रों की सुन्दरता के समान कमल पुष्प नहीं है, इस बात को कौन नहीं जानता? अर्थात् सब जानते हैं। अपनी इस अक्षमता को कमल भी जानता है। तभी तो अपने अपमान में व्यक्ति झेकर वह जल में जाकर छिपा गया है। यहाँ कवि प्रतीप अलंकार के सहारे यह कहना चाहता है कि नायिका के नेत्र कमल के पष्पों से अधिक मन्दर हैं।
8. भनई विद्यापति…………देइ रमाने।
व्याख्या-
प्रस्तुत पंक्तियाँ विद्यापति रचित पद की हैं। यहाँ कवि अपनी नायिका को यह बताना चहाता है कि तुम श्रेष्ठ युवती हो अर्थात् सामान्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा रूप अनुपम है। कवि की दृष्टि में रूप लक्ष्मी का प्रतीक होता है। उसमें सौन्दर्य, ऐश्वर्य और मंगल तीनों का भाव मिला होता है। जिस तरह लक्ष्मी किसी-किसी सौभाग्यशाली पर कृपा-करती हैं उसी तरह विधाता द्वारा सौन्दर्य-रूप-वैभव किसी-किसी को दिया जाता है।
vidyapati ke pad