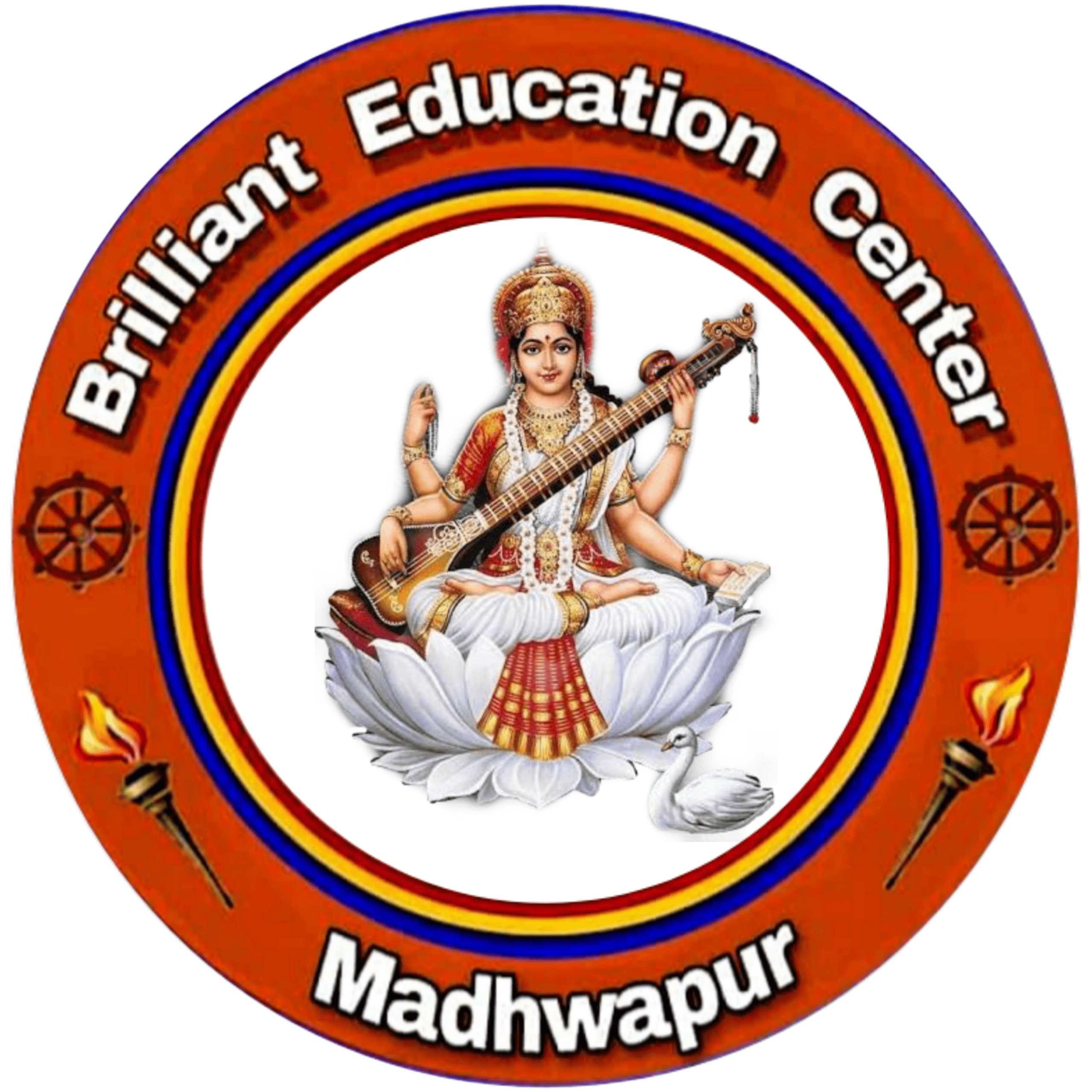कबीर के पद
1.
कबीर ने संसार को बौराया क्यों कहा है?
उत्तर-
kabir ke pad
म्परागत ढंग से भिन्न है, अत: लोगों को अच्छी नहीं लगती। इसलिए कबीर ने ऐसा कहा है कि यह संसार बौरा गया है, अर्थात पागल-सा हो गया है।
kabir ke pad
प्रश्न 2.
“साँच कहाँ तो मारन धावै, झूठे जग पतियाना” कबीर ने यहाँ किस सच और झूठ की बात कही है?
उत्तर-
कबीर ने बाह्याडंबरों से दूर रहकर स्वयं को पहचानने की सलाह दी है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। कबीर संसार के लोगों को ईश्वर और धर्म के बारे में सत्य बातें बताता है, ये सब परंपरागत ढंग से भिन्न है, अत: लोगों को यह पसंद नहीं है। संसार के लोग सच को सहन न करके झूठ पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार कबीर ने हिन्दू और मुसलमान दोनों के बाह्यडंबरों पर तीखा कटाक्ष किया है।
kabir ke pad
प्रश्न 3.
कबीर के अनुसार कैसे गुरु-शिष्य अन्तकाल में पछताते हैं? ऐसा क्यों होता है?
उत्तर-
कबीर के अनुसार इस संसार में दो तरह के गुरु और शिष्य मिलते हैं। एक कोटि है सदगुरु और सद् शिष्य की जिन्हें तत्त्व ज्ञान होता है, जो विवेकी होते हैं, जिन्हें जीव-ब्रह्म के सम्बन्ध का ज्ञान होता है, ऐसे सदगुरु और शिष्यों में सद् आचार भरते हैं। इनका अन्तर-बाह्य एक समान होता है। ये अहंकार शून्य होते हैं। गुरु-शिष्य की दूसरी कोटि है असद गुरु-और असद शिष्य की। इस सम्बन्ध में कबीर ने एक साखी में कहा है-किताबों की अलमारी
kabir ke pad
प्रश्न 4.
“हिन्दू कहै मोहि राम पियारा, तुर्क कहै रहिमाना
आपस में दोउ लरि-लरि मुए, मर्म न काहू जाना।
इन पंक्तियों का भावार्थ लिखें।
उत्तर-
प्रस्तुत पंक्तियाँ अपने समय के और अपनी तरह के अनूठे समाज-सुधारक चिंतक कबीर रचित पद से उद्धृत है। इन पंक्तियों में परम सत्ता के एक रूप का कथन हुआ है। यही मर्म है, यही अन्तिम सत्य है कि परम ब्रह्म, अल्लाह, गॉड सभी एक ही हैं। किन्तु अज्ञानतावश अलग-अलग धर्म सम्प्रदायों में बता मानव समाज अपने-अपने भगवान से प्यार करता है, दूसरे के भगवान को हेय समझता है। अपने भगवान के लिए अन्ध-भक्ति दर्शाता है। उनकी यह कट्टरता, बद्धमूलता, इतनी प्यारी होती है कि जरा-जरा सी बात पर धार्मिक भावनाएं आहत होने लगती हैं।
kabir ke pad
प्रश्न 5.
‘बहुत दिनन के बिछुरै माधौ, मन नहिं बांधै धीर’ यहाँ माधौ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है?
उत्तर-
कबीर निर्गुण-भक्ति के अनन्य उपासक थे। उन्होंने परमात्मा को कण-कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता में देखते हुए उसकी रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। कबीर ने ईश्वर को “माधौ” कहकर पुकारा है।
kabir ke pad
प्रश्न 6.
कबीर ने शरीर में प्राण रहते ही मिलने की बात क्यों कही है?
उत्तर-
प्रेम में यों तो सम्पूर्ण शरीर मन, प्राण सभी सहभागी होते हैं किन्तु आँखों की भूमिका अधिक होती है। विरह की दशा में आँखें लगातार प्रेमास्पद की राह देखती रहती हैं। विरही प्रेमी की आंकुलता-व्याकुलता का अतृप्ति का ज्ञापन आँखों से ही होता है फिर इसका क्या भरोसा कि मृत्यु के बाद यही शरीर पुनः प्राप्त हो। प्रेम यदि इसी जन्म और मनुष्य योनि में हुआ है, विरह की ज्वाला में यदि यही शरीर, मन, प्राण दग्ध हो रहे हैं तो फिर प्रेम को सार्थक्य भी तभी प्राप्त होगा जब शरीर में प्राण रहते इसी जन्म में प्रभु से मिलन हो जाए। विरह मिलन में बदल जाए। यही कारण है कि कबीर ने शरीर में प्राण रहते ही मिलते ही बात कही है।
प्रश्न 7.
कबीर ईश्वर की मिलने के लिए बहुत आतुर हैं। क्यों?
उत्तर-
हिन्दी साहित्य के स्वर्ण युग भक्तिकाल के निर्गुण भक्ति की ज्ञानमार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास ने ‘काचै भांडै नीर’ स्वयं को तथा ‘धीरज’ अर्थात् धैर्य की प्रतिमूर्ति ईश्वर को कहा है। अपनी व्याकुलता तथा प्रियतम से मिलकर एकाकार होने की उनकी उत्कंट लालसा उन्हें आतुर बना देती है। तादात्म्य की उस दशा में कवि अपने जीवन को कच्ची मिट्टी का घड़ा में भरा पानी माना है। यह शरीर नश्वर है। मृत्यु शाश्वत सत्य है कवि इन लौकिक दुखों (जीवन-मृत्यु) से छुटकारा पाकर ईश्वर की असीम सत्ता में विलीन होना चाहता है। अतः कबीर की ईश्वर से मिलने की आतुरता अतीव तीव्र हो गई है।
kabir ke pad
प्रश्न 8.
दूसरे पद के आधार पर कबीर की भक्ति-भावना का वर्णन अपने शब्दों में करें।
उत्तर-
हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग-1 में संकलित कबीर रचित द्वितीय पद कबीर की भक्ति भावना का प्रक्षेपक है। वस्तुत: कबीर की भक्ति- भावना को एक विशिष्ट नाम दिया है-“रहस्यवाद”। यह रहस्यवाद साहित्य की एक स्पष्ट भाव धारा है, जिसका किसी रहस्य से कोई लेना-देना नहीं है। आत्मा-परमात्मा को प्रणय-व्यापार, मिलन-विरह आदि रहस्यवाद का उपजीव्य है।किताबों की अलमारी
इस रहस्यवाद में कवि स्वयं को स्त्री या पुरुष मानकर ईश्वर, आराध्य या परम ब्रह्म के साथ अपने विभिन्न क्रिया व्यापारों, क्षणों और उपलब्धियों का अत्यंत प्रांजल, भाव प्रवण वर्णन करती है।
kabir ke pad
प्रश्न 9.
बलिया का प्रयोग सम्बोधन में हुआ है। इसका अर्थ क्या है?
उत्तर-
कबीर रचित पद में बलिया सम्बोधन शब्द आया है जिसका कोशगत अर्थ ‘बलवान’ है। किन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि कबीर भाषा के डिक्टेटर हैं। “बाल्हा” शब्द ‘बलिया’ का विकृत रूप है जिसका प्रयोग कबीर ने एक अन्य पद में किया है बाल्हा आओ हमारे गेह रे। कबीर के मत से बलिया का अर्थ सर्वशक्ति सम्पन्न परमपुरुष, भर्तार और पति ही है।
kabir ke pad
प्रश्न 10.
प्रथम पद में कबीर ने बाह्याचार के किन रूपों का जिक्र किया है? उन्हें अपने शब्दों में लिखें।
उत्तर-
परम्परा-भंजक; रूढ़ि-भंजक, समाज-सुधारक कबीर रचित प्रथम पद में हिन्दू-मुस्लिम दोनों ही सम्प्रदायों में व्याप्त आडम्बर पूर्ण बाह्याचारों का उल्लेख हुआ है।
तथाकथित नेमी द्वारा (नियमों का कठोरता से अनुपालन करने वाले) प्रात:काल प्रत्येक ऋतु और अवस्था में स्नान करना, पाहन (पत्थर) की पूजा करना, आसन मारकर बैठना और समाधि लगाना पितरों (पितृ) की पूजा, तीर्थाटन करना, विशेष प्रकार की टोपी, पगड़ी को धारण करना, तरह-तरह के पदार्थों की माला (तुलसी, चन्दन, रुद्राक्ष और पत्थरों की मालाएँ) माथे पर विभिन्न रंगों और रूपों में, गले में कानों के आस-पास बाहुओं पर तिलक-छापा लगाना ये सभी बाह्याडम्बर है। इनका विरोध मुखर स्वर में कबीर ने किया है।
kabir ke pad
प्रश्न 11.
कबीर धर्म उपासना के आडंबर का विरोध करते हुए किसके ध्यान पर जोर देते हैं?
उत्तर-
संत कबीर ने हिन्दू और मुसलमानों के ढोंग-आडंबरों पर करारी चोट की है। उन्होंने धर्म के बाहरी विधि विधानों, कर्मकांडों-जप, माला, मूर्तिपूजा, रोजा, नमाज आदि का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि हिन्दू और मुसलमान आत्म-तत्त्व और ईश्वर के वास्तविक रहस्य से अपरिचित हैं, क्योंकि मानवता के विरुद्ध धार्मिक कट्टर और आडम्बरपूर्ण कोई भी व्यक्ति अथवा : .. धर्म ईश्वर की परमसत्ता का अनुभव नहीं कर सकता।
कबीर ने स्वयं (आत्मा) को पहचानने पर बल देते हुए कहा है कि यही ईश्वर का स्वरूप है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है।
kabir ke pad
प्रश्न 12.
आपस में लड़ते-मरते हिन्दू और तर्क को किस मर्म पर ध्यान देने की सलाह कवि देता है?
उत्तर-
मुगल बादशाह बाबर के जमाने से हिन्दू-मुसलमान अपने पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के कारण लड़ते-मरते चले आ रहे हैं। साम्प्रदायिक सौहार्द्र की जगह साम्प्रदायिकता का जहर पूरे समाज में घुला हुआ है। दोनों ही सम्प्रदायों का तथाकथित पढ़ा-लिखा और अनपढ़ तबका ‘ईश्वर’ की सत्ता, अवस्थिति की वस्तु स्थिति से अनवगत है। मूल चेतना, मर्म का ज्ञान किसी को नहीं है।
वेद-पुराण, कुरान, हदीश लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों पर ईश्वर के स्वरूप, उसके प्रभाव और सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होने की बात कही गयी है। kabir ke pad
प्रश्न 13.
“सहजै सहज समाना” में सहज शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। इस प्रयोग की सार्थकता स्पष्ट करें।
उत्तर-
मध्यकालीन भारत में भक्ति की क्रांतिकारी भाव धारा को जन-जन तक पहुँचाने वाले भक्त कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को ‘सहजै सहज समाना’ शब्द का दो बार प्रयोग किया है। प्रस्तुत शब्द में कबीर द्वारा बाह्याडंबरों की अपेक्षा स्वयं (आत्मा) को पहचानने की बात कही गई है। अपने शब्दों में कबीर ने ये बाह्याडंबर बताए हैं-पत्थर पूजा, कुरान पढ़ाना, शिष्य बनाना, तीर्थ-व्रत, टोपी-माला पहनना, छापा-तिल, लगाना, पीर औलिया की बातें मानना आदि।
kabir ke pad
प्रश्न 14.
कबीर ने भर्म किसे कहा है?
उत्तर-
कबीर के अनुसार अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्य अज्ञानता के अंधकार में डूब जाते हैं। इनके गुरु भी अज्ञानी होते हैं; वे घर-घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं। मिथ्याभिमान के परिणामस्वरूप लोग विषय-वासनाओं की आग से झुलस रहे हैं। कवि का कहना है कि धार्मिक आडम्बरों में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही ईश्वर की परम सत्ता से अपरिचित हैं। इनमें कोई भी प्रभु के प्रेम का सच्चा दीवाना नहीं है।
कबीर ने इन बाह्याडम्बरों के ‘भर्म’ को भुलाकर स्वयं (आत्मा) को पहचानने की सलाह देते हुए कहा है कि आत्मा का ज्ञान की सच्चा ज्ञान है। ईश्वर हर साँस में समाया हुआ है अर्थात् सच्ची अनुभूति और आत्म-साक्षात्कार के बल पर ईश्वर को पल भर की तलाश में ही पाया जा सकता है।
kabir ke pad
प्रश्न 2.
दोनों पदों में जो विदेशज शब्द आये हैं उनकी सूची बनाएँ एवं उनका अर्थ लिखें।
उत्तर-
कबीर रचित पद द्वय में निम्नलिखित विदेशज (विदेशी) शब्द आये हैं, जिनका अर्थ अग्रोद्धत है
पीर-धर्मगुरु; औलिया-संत; कितेब-किताब, पुस्तक; कुरान-इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ; मुरीद-शिष्य, चेला, अनुयायी; तदबीर-उपाय, उद्योग, कर्मवीरता; खवरि-सूचना, ज्ञान; तुर्क-इस्लाम धर्म के अनुयायी, तुर्की देश के निवासी; रहिमाना-रहमान-रहम दया करने वाला अल्ला।किताबों की अलमारी
kabir ke pad
प्रश्न 3.
पठित पदों से उन शब्दों को चुनें निम्नलिखित शब्दों के लिए आये हैं
उत्तर-
आँख-नैन; पागल-वौराना (बौराया); धार्मिक-धरमी; बर्तन-भांडे, वियोग-विरह, आग-अगिनि, रात-निस।
kabir ke pad
प्रश्न 4.
नीचे प्रथम पद से एक पंक्ति दी जा रही है, आप अपनी कल्पना से तुक मिलते हुए अन्य पंक्तियाँ जोड़ें- “साँच कहो तो मारन धावै, झूठे जग पतियाना।”
उत्तर-
साँच कहो तो मारन धावै झूठे जग पतियाना,
मर्म समझ कर चेत ले जल्दी घूटे आना-जाना,
जीवन क्या इतना भर ही है रोना हँसना खाना,
हिय को साफ तू कर ले पहले, बसे वहीं रहिमान।
छोड़ सके तो गर्व छोड़ दे राम बड़ा सुलिताना,
भाया मोह की नगरी से जाने कब पड़ जाय जाना”
चेत चेत से मूरख प्राणी पाछे क्या पछि ताना।
(kabir ke pad)
प्रश्न 5.
कबीर की भाषा को पंचमेल भाषा कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीर की भाषा पर अपने शिक्षक से चर्चा करें अथवा कबीर की भाषा-शैली पर एक सार्थक टिप्पणी दें।
उत्तर-
“लिखा-लिखि की है नहीं देखा देखी बात’ “की उद्घोषणा करने वाले भाषा के डिक्टेटर और वाणी के नटराज कबीर की भाषा-शैली कबीर की ही प्रतिमूर्ति है। कबीर बहु-श्रुत और परिव्राजक संत कवि थे। हिमालय से हिन्द महासागर और गुजरात से मेघालय तक फैले उनके अनुयायियों द्वारा किये गये कबीर की रचनाओं के संग्रह में प्रक्षिप्त क्षेत्रियता का निदर्शन इस बात का सबल प्रमाण है कि कबीर “जैसा देश वैसी वाणी, शैली’ के प्रयोक्ता थे।
(kabir ke pad)
प्रश्न 6.
प्रथम पद में अनुप्रास अलंकार के पाँच उदाहरण चुनें।
उत्तर-
नेमि देखा धरमी देखा-पंक्त में ‘मि’ वर्ण और देखा शब्द की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। जै पखानहि पूजै में प वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार पीर पढ़े कितेब कुराना में क्रमशः प और क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। उनमें उहै में उ वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार। पीतर पाथर पूजन में प वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार उपस्थित है।
kabir ke pad
प्रश्न 7.
दूसरे पद में ‘विरह अगिनि’ में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के चार अन्य उदाहरण दें।
उत्तर-
रूपक अलंकार के चार अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं ताराघाट, रघुवर-बाल-पतंग, चन्द्रमुखी, चन्द्रबदनी, मृगलोचनी।
kabir ke pad
प्रश्न 8.
कारक रूप स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
झठे-झूठ को-द्वितीय तत्पुरुष, पखानहि-पत्थर को द्वितीया तत्पुरुष; सब्दहि-शब्द को-द्वितीय-तत्पुरुष, खबरि-सूचना ही में-सम्प्रदान तत्पुरुष; कारनि-कारण से-अपादान, तत्पुरुष, भांडै-भांड में-अधिकरण तत्पुरुष।
kabir ke pad
प्रश्न 9.
पाठ्य-पुस्तक में संकलित कबीर रचित पद “संतौ देखो जग बौराना’ का भावार्थ लिखें।
उत्तर-
प्रश्न 10. पाठ्य-पुस्तक में संकलित कबीर रचित द्वितीय पद का भावार्थ प्रस्तुत करें। उत्तर-द्वितीय पद का भावार्थ देखें।
प्रश्न 1.
कबीर की विरह-भावना पर प्रकाश डालें।
उत्तर-
कबीर परमात्मा से प्रेम करने वाले भक्त हैं। उनकी प्रीति पति-पत्नी भाव की है। परमात्मा रूपी पति से मिलन नहीं होने के कारण वे विरहिणी स्त्री की भाँति विरहाकुल रहते हैं। ये प्रियतम के दर्शन हेतु दिन-रात आतुर रहते हैं। उनके नेत्र उन्हें देखने के लिए सदैव आकुल रहते हैं। वे विरह की आग में सदैव जलते रहते हैं। एक वाक्य में उनकी दशा यही है कि “तलफै बिनु बालम मोर जिया। दिन नहिं चैन, रात नहिं, निंदिया तरप तरप कर भोर किया।”
kabir ke pad
प्रश्न 1.
कबीर विरह की दशा में क्या अनुभव करते हैं?
उत्तर-(kabir ke pad)
कबीर को विरह की अग्नि जलाती है, आतुरता और उद्वेग पैदा करती है तथा मन धैर्य से रहित हो जाता है।
(kabir ke pad)
प्रश्न 2.
कबीर परमात्मा से क्या चाहते हैं?
उत्तर-
कबीर परमात्मा का दर्शन चाहते हैं, विरह-दशा की समाप्ति और मिलन का सुख चाहते हैं।
प्रश्न 3.
कबीर के अनुसार हिन्दू-मुस्लिम किस मुद्दे पर लड़ते हैं? उत्तर-हिन्दू-मुसलमान नाम की भिन्नता और उपासना की भिन्नता को लेकर लड़ते हैं। प्रश्न 4. कबीर की दृष्टि में नकली उपासक क्या करते हैं?
उत्तर-
नकली उपासक नियम-धरम का विधिवत पालन करते हैं, माला-टोपी धारण करते हैं, आसन लगाकर उपासना करते हैं, पीपल-पत्थर पूजते हैं, तीर्थव्रत करते हैं तथा भजन-कीर्तन गाते हैं।
kabir ke pad
प्रश्न 5.
कबीर की दृष्टि में नकली गुरु लोग क्या करते हैं?
उत्तर-
नकली गुरु लोग किताबों में पढ़ें मन्त्र देकर लोगों को शिष्य बनाते हैं और ठगते हैं।
इन्हें अपने ज्ञान, महिमा तथा गुरुत्व का अभिमान रहता है लेकिन वास्तव में ये आत्मज्ञान से रहित मूर्ख, ठग और अभिमानी होते हैं।
kabir ke pad
प्रश्न 6.
कबीर के अनुसार ईश्वर-प्राप्ति का असली मार्ग क्या है?
उत्तर-
ईश्वर-प्राप्ति का असली मार्ग है आत्मज्ञान अर्थात् अपने को पहचानता और अपनी सत्ता को ईश्वर से अभिन्न मानना तथा ईश्वर से सच्चा प्रेम करना।
kabir ke pad
प्रश्न 7.
कबीरदास ने प्रथम पद में किसकी व्यर्थता सिद्ध की है?
उत्तर-
कबीरदास ने अपने प्रथम पद में पत्थर पूजा, तीर्थाटन और छाप तिलक को व्यर्थ बताया है।
प्रश्न 8.
कबीर ने दूसरे पद में बलिध का प्रयोग किसके लिए किया है?
उत्तर-
कबीरदास ने अपने दूसरे पद में बलिध का प्रयोग परमात्मा और सर्वशक्तिमान के लिए किया है।
kabir ke pad
प्रश्न 9.
कबीर के दृष्टिकोण में सारणी या सबद गाने वाले को किसकी खबर नहीं है?
उत्तर-
कबीरदास ने दृष्टिकोण में सारणी या सबद गाने वाले को स्वयं अपनी खबर नहीं है
kabir ke pad
1. संतो देखत जग बौराना…………नमें कछु नहिं ज्ञाना।
व्याख्या-
प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने धार्मिक क्षेत्र में उलटी रीति और संसार के लोगों के बावलेपन का उल्लेख किया है। वे संतों अर्थात् सज्जन तथा ज्ञान-सम्पन्न लोगों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि संतो! देखो, यह संसार बावला या पागल हो गया है? इसने उल्टी राह पकड़ ली है। जो सच्ची बात कहता है उसे लोग मारने दौड़ते हैं। इसके विपरीत जो लोग गलत और झूठी बातें बताते हैं उन पर वे विश्वास करते हैं। मैंने धार्मिक नियमों और विधि-विधानों का पालन करने वाले अनेक लोगों को देखा है। वे प्रातः उठकर स्नान करते हैं, तथा मंदिरों में जाकर पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं। मगर उनके पास तनिक भी ज्ञान नहीं है। वे अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं और उसकी आवाज को मारते हैं, अर्थात् अनसुनी करते हैं, अर्थात् अनसुनी करते हैं, सारांशतः कबीर कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग केवल बाहरी धर्म-कर्म और नियम-आचार जानते हैं जबकि अन्त: ज्ञान से पूर्णतः शून्य हैं।
kabir ke pad
2. बहुतक देखा पीर औलिया…………..उनमें उहै जो ज्ञाना।
व्याख्या-
कबीरदास जी ने अपने पद की प्रस्तुत पंक्तियों में मुसलमानों के तथाकथित पीर और औलिया के आचरणों का परिहास किया है। वे कहते हैं कि मैंने अनेक पीर-औलिये को देखा है जो नित्य कुरान पढ़ते रहते हैं। उनके पास न तो सही ज्ञान होता है और न कोई सिद्धि होती है फिर भी वे लोगों को अपना मुरीद यानी अनुगामी या शिष्य बनाते और उन्हें उनकी समस्याओं के निदान के उपाय बताते चलते हैं। यही उनके ज्ञान की सीमा है। निष्कर्षतः कबीर कहना चाहते हैं कि ये पीर-औलिया स्वतः अयोग्य होते हैं लेकिन दूसरों को ज्ञान सिखाते फिरते हैं। इस तरह ये लोग ठगी करते हैं।
kabir ke pad
3. आसन मारि डिंभ धरि…………….आतम खबरि न जाना।
व्याख्या-
कबीरदास जी का स्पष्ट मत है कि जिस तरह मुसलमानों के पीर औलिया ठग हैं उसी तरह हिन्दुओं के पंडित ज्ञान-शूल। वे कहते हैं कि ये नकली साधक मन में बहुत अभिमान रखते हैं और कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ लेकिन होते हैं ज्ञान-शूल। ये पीपल पूजा के रूप में वृक्ष पूजते हैं, मूर्ति पूजा के रूप में पत्थर पूजते हैं। तीर्थ कर आते हैं तो गर्व से भरकर अपनी वास्तविकता भूल जाते हैं। ये अपनी अलग पहचान बताने के लिए माला, टोपी, तिलक, पहचान चिह्न आदि धारण करते हैं
kabir ke pad
4. हिन्दु कहै मोहि राम पियारा………….मरम न काहू जाना।
व्याख्या-
कबीर कहते हैं कि हिन्दू कहते हैं कि हमें राम प्यारा है। मुसलमान कहते हैं कि हमें रहमान प्यारा है। दोनों इन दोनों को अलग-अलग अपना ईश्वर मानते हैं और आपस में लड़ते तथा मार काट करते हैं। मगर, कबीर के अनुसार दोनों गलत हैं। राम और रहमान दोनों एक सत्ता के दो नाम हैं। इस तात्त्विक एकता को भूलकर नाम-भेद के कारण दोनों को भिन्न मानकर आपस में लड़ना मूर्खता है। अत: दोनों ही मूर्ख हैं जो राम-रहीम की एकता से अनभिज्ञ हैं।
kabir ke pad
5. घर घर मंत्र देत…………….सहजै सहज समाना।
व्याख्या-
कबीरदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि कुछ लोग गुरु बन जाते हैं मगर मूलतः वे अज्ञानी होते हैं। गुरु बनकर वे अपने को महिमावान समझने लगते हैं। महिमा के इस अभिमान से युक्त होकर वे घर-घर घूम-घूम कर लोगों को गुरुमंत्र देकर शिष्य बनाते चलते हैं। कबीर के मतानुसार ऐसे सारे शिष्य गुरु बूड़ जाते हैं; अर्थात् पतन को प्राप्त करते हैं और अन्त समय में पछताते हैं। इसलिए कबीर संतों को सम्बोधित करने के बहाने लोगों को समझाते हैं कि ये सभी लोग भ्रमित हैं, गलत रास्ते अपनाये हुए हैं।
kabir ke pad
6. हो बलिया कब देखेंगी…………..न मानें हारि।
व्याख्या-
प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने ईश्वर के दर्शन पाने की अकुलाहट भरी इच्छा व्यक्त की है। वे कहते हैं कि प्रभु मैं तुम्हें कब देखूगा? अर्थात् तुम्हें देखने की मेरी इच्छा कब पूरी होगी, तुम कब दर्शन दोगे? मैं दिन-रात तुम्हारे दर्शन के लिए आतुर रहता हूँ। यह इच्छा मुझे इस तरह व्याप्त किये हुई है कि एक पल के लिए भी इस इच्छा से मुक्त नहीं हो पाता हूँ।
मेरे नेत्र तुम्हें चाहते हैं और दिन-रात प्रतीक्षा में ताकते रहते हैं। नेत्रों की चाह इतनी प्रबल है कि ये न थकते हैं और न हार मानते हैं। अर्थात् ये नेत्र जिद्दी हैं
(kabir ke pad)
7. “बिरह अगिनि तन……………..जिन करहू बधीर।”
व्याख्या-
प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी ! तुम्हारे वियोग की अग्नि में यह शरीर जल रहा है, तुम्हें पाने की लालसा आग की तरह मुझे दग्ध कर रही है। ऐसा मानकर तुम विचार कर लो कि मैं दर्शन पाने का पात्र हूँ या उपेक्षा का?
कबीरदास जी अपनी विरह-दशा को बतला कर चुप नहीं रह जाते हैं? वे एक वादी अर्थात् फरियादी करने वाले व्यक्ति के रूप में अपना वाद या पक्ष या पीड़ा निवेदित करते हैं और प्रार्थना. करते हैं कि तुम मेरी पुकार सुनो, बहरे की तरह अनसुनी मत करो। पंक्तियों की कथन-भगिमा की गहराई में
(kabir ke pad)
8. तुम्हे धीरज मैं आतुर…………….आरतिवंत कबीर।
व्याख्या-
अपने आध्यात्मिक विरह-सम्बन्धी पद की प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर अपनी तुलना आतुरता और ईश्वर की तुलना धैर्य से करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी ! तुम धैर्य हो और मैं आतुर। मेरी स्थिति कच्चे घड़े की तरह है। कच्चे घड़े में रखा जल शीघ्र घड़े को गला कर बाहर निकलने लगता है। उसी तरह मेरे भीतर का धैर्य शीघ्र समाप्त हो रहा है अर्थात् मेरा मन अधीर हो रहा है। आप से बहुत दिनों से बिछुड़ चुका ह

matric exam