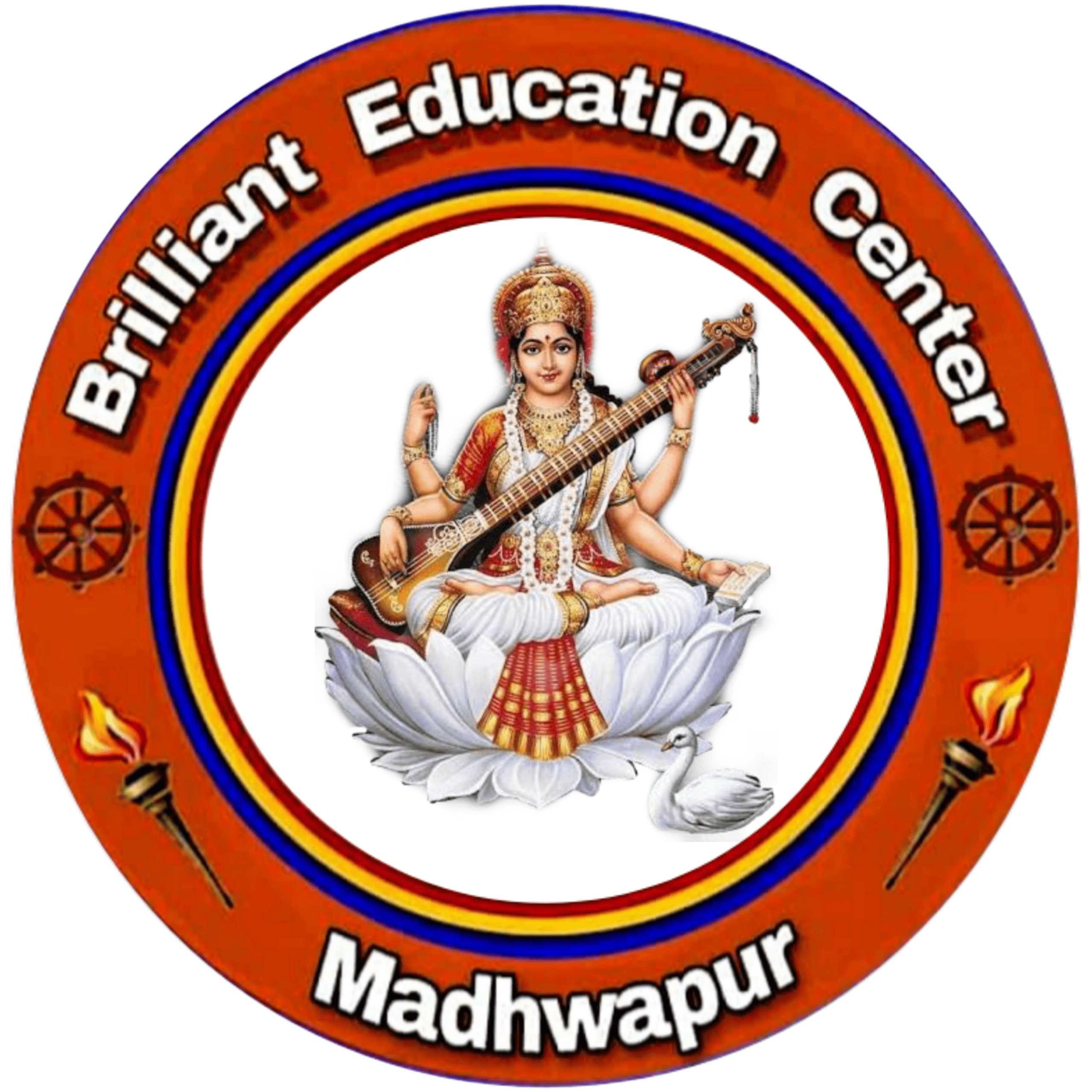Skip to contentBihar Board class 9 Political Science chapter 4 – वस्तुनिष्ठ प्रश्न
प्रश्न 1. चुनाव का मतलब है
(क) पैसा कमाना
(ख) राजनीतिक प्रतिस्पर्धा
(ग) राजनीतिक खेल
(घ) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (ख) राजनीतिक प्रतिस्पर्धा
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 2. लोकतांत्रिक देश में क्या नियमित होता है ?
(क) युद्ध
(ख) आपसी संघर्ष
(ग) चुनाव
(घ) खेती
उत्तर- (ग) चुनाव
प्रश्न 3. लोकसभा में सीटों की संख्या निम्नलिखित में से क्या है ?
(क) 500
(ख) 520
(ग) 525
(घ) 543
उत्तर- (घ) 543
प्रश्न 4. बिहार विधान सभा में विधायकों की सीटें हैं
(क) 243
(ख) 253
(गे) 250
(घ) 153
उत्तर- (क) 243
प्रश्न 5. लोकसभा में अनुसूचित जन जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित
(क) 60
(ख) 41
(ग) 40
(घ) 20
उत्तर- (ख) 41
प्रश्न 6. लोकसभा एवं विधान सभा के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है ?
(क) 20 वर्ष
(ख) 18 वर्ष
(ग) 21 वर्ष
(घ) 25 वर्ष
उत्तर- (क) 20 वर्ष
प्रश्न 7. चुनावी मतदाता होने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी’ चाहिए?
(क) 18 वर्ष
(ख) 21 वर्ष
(ग) 25 वर्ष
(घ) 30 वर्ष
उत्तर- (क) 18 वर्ष
प्रश्न 8. 1971 ई० में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में नारा दिया था.
(क) लोकतंत्र बचाओ
(ख) तेलगू स्वाभिमान
(ग) गरीबी हटाओ
(घ) अमीरी मिटाओ
उत्तर- (ग) गरीबी हटाओ
प्रश्न 9. 1977 ई. में जनता पार्टी ने देशभर में नारा दिया था
(क) गरीबी मिटाओ
(ख) गरीबी हटाओ
(ग) अमीरी मिटाओ
(घ) लोकतंत्र बचाओ
उत्तर- (घ) लोकतंत्र बचाओ
प्रश्न 10. एक विधान सभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है ?
(क) 5 लाख
(ख) 10 लाख
(ग) 15 लाख
(घ) 20 लाख
उत्तर- (ख) 10 लाख
प्रश्न 11. एक लोकसभा का उम्मीदवार वैधानिक ढंग से अपने चुनाव अभियान में अधिकतम कितनी धनराशि खर्च कर सकता है ?
(क) 5 लाख
(ख) 8 लाख
(ग) 20 लाख
(घ) 25 लाख
उत्तर- (घ) 25 लाख
प्रश्न 12. लोकसभा के चुनाव हेतु सम्पूर्ण भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है ?
(क) 250
(ख) 324
(ग) 420
(घ) 543
उत्तर- (क) 250
प्रश्न 13. चुनाव प्रचार में निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध नहीं है ?
(क) धर्म के नाम पर प्रचार
(ख) सरकारी वाहन का प्रयोग
(ग) सरकार को नीतिगत फैसला करना
(घ) सीधा-सादा प्रचार
उत्तर- (क) धर्म के नाम पर प्रचार
प्रश्न 14. लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं ?
(क) 70
(ख) 72
(ग) 75
(घ) 79
उत्तर- (घ) 79
प्रश्न 15. बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं ?
(क) 5
(ख) 8
(ग) 0 (शून्य)
(घ) 10
उत्तर- (घ) 10
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
रिक्त स्थान की पूर्ति करें
प्रश्न 1. राजनीतिक पार्टियों के बीच ………….. होता है।
उत्तर- प्रतिस्पर्धा
प्रश्न 2. अगर प्रतिस्पर्धा नहीं रहे तो चुनाव ………….हो जायेंगे।
उत्तर- बेमानी
प्रश्न 3. नियमित अंतराल पर चुनावी मुकाबलों का लाभ ……………………….. और नेताओं को मिलता है।
उत्तर- राजनीतिक दलों
प्रश्न 4. लोकतांत्रिक चुनाव की यह विशेषता है कि हर वोट को ……………….. .. का आधार बनाया जाता है।
उत्तर- मूल्य
प्रश्न 5. निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के लिए जनसंख्या एवं …………………. …. का आधार बनाया जाता है।
उत्तर- क्षेत्रफल
प्रश्न 6. महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर सिर्फ ………………. . चुनाव लड़ सकती
उत्तर- महिलाएँ
प्रश्न 7. भारत में चुनाव प्रचार के लिए आमतौर पर ……………… . का समय दिया जाता है।
उत्तर- दो सप्ताह
प्रश्न 8. …………….. में आन्ध्र प्रदेश में तेलगू स्वाभिमान का नारा दिया गया था।
उत्तर- 1983
प्रश्न 9. ……………. में झारखंड में ‘झारखंड बचाओ’ का नारा दिया गया था।
उत्तर- 2000
प्रश्न 10. भारतीय संविधान ने चुनावों की निष्पक्षता की जाँच के लिए स्वतंत्र चुनाव ………. का गठन किया है।
उत्तर- आयोग
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 11. चुनाव आयोग को …………….. कहते हैं
उत्तर- भारतीय निर्वाचन आयोग
प्रश्न 12. चुनाव का स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का आखिरी पैमाना उसके …………. हैं।
उत्तर- नतीजे
प्रश्न 13. नगर परिषद् से चुने गए प्रतिनिधियों को नगर …………….. कहते हैं।
उत्तर- पार्षद
प्रश्न 14. गाँवों में आप कहते सुनेंगे कि …………….. ने हमारे घरों को बाँट दिया है।
उत्तर- पार्टी-पॉलिटिक्स
प्रश्न 15. चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नामों की ……………… करते हैं।
उत्तर- घोषणा
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
Bihar Board class 9 Political Science chapter 4 – अतिलघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. मताधिकार किसे कहते हैं ?
उत्तर- राज्य की ओर से नागरिकों को जो मत देने का अधिकार दिया गया है उसे मताधिकार कहते हैं।
प्रश्न 2. मतदान का क्या अर्थ है ?
उत्तर- निर्वाचन के समय कोई व्यक्ति उसमें भाग लेकर अपने मत का प्रयोग करते हैं उसे मतदान कहते हैं
प्रश्न 3. मतदाता किसे कहते हैं ?
उत्तर- चुनाव में मतदान करनेवाले व्यक्ति को मतदाता कहते हैं।
प्रश्न 4. चुनाव का प्रमुख उद्देश्य क्या है ?
उत्तर- जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधियों का चुनाव करे।
प्रश्न 5. चुनाव नियमित रूप से क्यों होना चाहिए?
उत्तर- इसलिए ताकि मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अवसर मिलता रहे।
प्रश्न 6. चुनाव चिह्न का क्या महत्व होता है ? .
उत्तर- भारत के अधिकांश मतदाता अनपढ़ हैं जिस कारण मतदाता चुनाव चिह्न को पहचान कर अपनी पसंद से मतदान कर सकें।
प्रश्न 7. लोकतांत्रिक देश में चुनाव से क्या अभिप्राय है ?
उत्तर- लोकतांत्रिक देश में चुनाव वास्तव में लोकतंत्र का आधार है। चुनाव के द्वारा ही लोकतंत्र में प्रत्याशी चयनित किए जाते हैं।
प्रश्न 8. मतदान केन्द्रों पर चुनाव सम्पन्न करने का उत्तरदायित्व किस पर होता है ?
उत्तर- पीठासीन पदाधिकारी पर
प्रश्न 9. मतदाताओं की अंगुली पर एक अमिट स्याही क्यों लगा दी जाती है?
उत्तर- ताकि वह दुबारा वोट न दे सके।
प्रश्न 10. भारतीय चुनाव प्रणाली की एक विशेषता को लिखें।
उत्तर- नियमित चुनाव प्रणाली ।
प्रश्न 11. मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ?
उत्तर- राष्ट्रपति
प्रश्न 12. भारत का चुनाव आयोग कैसा है ?
उत्तर- काफी शक्तिशाली और स्वतंत्र ।
प्रश्न 13. किन लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया है ?
उत्तर- गंभीर प्रकार के अपराधी, पागल एवं दिवालिया को मताधिकार नहीं दिया गया।
प्रश्न 14. निर्वाचन क्षेत्र क्या है ?
उत्तर- एक खास भौगोलिक क्षेत्र जहाँ से मतदाता एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं।
प्रश्न 15. आदर्श चुनाव आचार संहिता क्या है ?
उत्तर- चुनाव की अधिसूचना के पश्चात् पार्टियाँ और उम्मीदवारों द्वारा अनिवार्य रूप से माने जाने वाले कायदे-कानून और दिशा-निर्देश को आचार संहिता कहते हैं।
लघु उत्तरीय प्रश्न
प्रश्न 1. भारत में मतदाता की कौन-सी तीन योग्यताएँ होनी चाहिए ?
उत्तर- भारत में मतदाता की तीन मुख्य योग्यताएँ हैं:-
भारतीय नागरिकता: व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।
न्यूनतम आयु: मतदान की तिथि तक व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
मतदाता सूची में पंजीकरण: व्यक्ति का नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया होना चाहिए।
प्रश्न 2. भारत में संसदीय चुनाव के उम्मीदवार की कोई तीन योग्यताएँ बताएँ।
उत्तर- संसदीय चुनाव के उम्मीदवार की तीन प्रमुख योग्यताएँ हैं:-
नागरिकता: उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
न्यूनतम आयु: लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए।
आपराधिक रिकॉर्ड: उम्मीदवार के खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा, उम्मीदवार को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और दिवालिया घोषित नहीं किया गया होना चाहिए।
प्रश्न 3. चुनाव प्रणाली क्या है ?
उत्तर- चुनाव प्रणाली वह संवैधानिक व्यवस्था है जिसके द्वारा लोकतांत्रिक देश में नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। इसमें मतदान, मतगणना, और परिणाम घोषणा की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। भारत में, यह प्रणाली संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए उपयोग की जाती है। चुनाव प्रणाली का उद्देश्य जनता की इच्छा को प्रतिबिंबित करना और शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
प्रश्न 4. चुनाव को आवश्यक क्यों माना गया है ?
उत्तर- चुनाव लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। यह जनता को नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों का मूल्यांकन करने और उन्हें बदलने का अवसर देता है। चुनाव सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। ये शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की अनुमति देते हैं और विभिन्न राजनीतिक विचारों को अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार, चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत और स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
प्रश्न 5. राजनैतिक प्रतिस्पर्धा से आमलोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
उत्तर- राजनैतिक प्रतिस्पर्धा का आम लोगों पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक पक्ष में, यह जनता को विभिन्न नीतिगत विकल्प प्रदान करती है और नेताओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। हालांकि, नकारात्मक पहलू में, यह कभी-कभी समुदायों में विभाजन पैदा कर सकती है और राजनीतिक दलों के बीच कटु संबंध बना सकती है। आदर्श स्थिति में, स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र को मजबूत करती है, लेकिन इसे नैतिक और सम्मानजनक तरीके से संचालित किया जाना चाहिए।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 6. क्या हमारे देश में चुनाव लोकतांत्रिक है ?
उत्तर- हाँ, भारत में चुनाव प्रक्रिया मूल रूप से लोकतांत्रिक है। इसके प्रमुख लक्षण हैं:-
नियमित चुनाव: लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर पाँच साल बाद होते हैं।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार: 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार है।
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव: स्वतंत्र चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है।
बहुदलीय प्रणाली: विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं।
गुप्त मतदान: मतदाताओं की गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है।
ये विशेषताएँ भारतीय चुनाव प्रणाली के लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रदर्शित करती हैं।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 7. निर्वाचन क्षेत्र क्या है ? इसके निर्माण का क्या आधार है ?
उत्तर- निर्वाचन क्षेत्र एक भौगोलिक इकाई है जहाँ से मतदाता एक प्रतिनिधि चुनते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, ताकि हर प्रतिनिधि लगभग समान संख्या के लोगों का प्रतिनिधित्व करे। उदाहरण के लिए, लोकसभा के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा गया है। निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यह व्यवस्था प्रतिनिधि लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 8. संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित क्षेत्र की बात क्यों सोची?
उत्तर- संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित क्षेत्रों की व्यवस्था इन कारणों से की:-
समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: ताकि समाज के हर वर्ग की आवाज संसद और विधानसभाओं में पहुंचे।
सामाजिक न्याय: सदियों से वंचित रहे समूहों को राजनीतिक शक्ति में हिस्सेदारी देना।
संसाधनों की कमी की भरपाई: इन समूहों के पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन न होने की स्थिति में भी उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
लोकतंत्र को मजबूत बनाना: सभी वर्गों की भागीदारी से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधिक और मजबूत बनाना।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 9. भारत में कौन ऐसा राज्य है जहाँ स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आधी सीटें आरक्षित कर दी गयीं हैं ?
उत्तर- बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की हैं। यह आरक्षण पंचायतों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में लागू है। इन आरक्षित सीटों में से कुछ अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। इस नीति का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना और उनका सशक्तिकरण करना है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 10. मतदाता सूची का क्या तात्पर्य है ?
उत्तर- मतदाता सूची एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसमें किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं के नाम दर्ज होते हैं। यह सूची चुनाव आयोग द्वारा तैयार और नियमित रूप से अपडेट की जाती है। इसमें मतदाताओं का नाम, आयु, लिंग और पता जैसी जानकारियाँ शामिल होती हैं। मतदाता सूची का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र व्यक्ति ही मतदान कर सकें और प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार मतदान करे।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 11. चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सही पहचान के लिए कितने प्रकार के पहचानों को वैध माना है ?
उत्तर- चुनाव आयोग ने मतदाताओं की पहचान के लिए 14 प्रकार के दस्तावेजों को वैध माना है। इनमें शामिल हैं:-
मतदाता पहचान पत्र (सबसे प्राथमिक)
आधार कार्ड
पासपोर्ट
ड्राइविंग लाइसेंस
पैन कार्ड
सरकारी/अर्ध-सरकारी कर्मचारियों के फोटो पहचान पत्र
बैंक/डाकघर पासबुक (फोटो सहित)
किसान पासबुक
श्रम मंत्रालय की योजनाओं के तहत जारी फोटो पहचान पत्र
पेंशनभोगियों के फोटो पहचान पत्र
इन दस्तावेजों का उपयोग मतदाताओं की सटीक पहचान सुनिश्चित करने और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किया जाता है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 12. चुनाव का प्रमुख उद्देश्य क्या है ?
उत्तर- चुनाव का प्रमुख उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। यह जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने का अवसर देता है। चुनाव सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं और शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाते हैं। यह विभिन्न राजनीतिक दलों और उनकी नीतियों के बीच तुलना करने का मौका देता है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण का माध्यम भी है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 13. वे कौन-कौन से ऐसे प्रतिबंधित कार्य हैं जिन्हें चुनाव के समय उम्मीदवार या पार्टी नहीं कर सकती ? अथवा, किस स्थिति में चुनाव रद्द घोषित हो सकता है ?
उत्तर- चुनाव के दौरान निम्नलिखित कार्य प्रतिबंधित हैं:-
मतदाताओं को रिश्वत देना या धमकाना
सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग
निर्धारित सीमा से अधिक धन खर्च करना
धार्मिक या जातीय भावनाओं का उपयोग
मतदान केंद्रों के पास प्रचार करना
यदि कोई उम्मीदवार इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका चुनाव रद्द किया जा सकता है। गंभीर उल्लंघन के मामले में पूरे निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव रद्द हो सकता है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 14. चुनाव के समय ‘आदर्श-आचार संहिता’ लागू होती है। वह क्या है?
उत्तर- आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट है। इसके मुख्य बिंदु हैं:-
धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग न करना
सरकारी संसाधनों का चुनावी लाभ के लिए उपयोग न करना
चुनाव की घोषणा के बाद बड़ी नीतिगत घोषणाएँ न करना
जाति या धर्म के आधार पर वोट न माँगना
शांतिपूर्ण और नैतिक तरीके से प्रचार करना
यह संहिता निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 15. चुनाव घोषणा पत्र क्या है ?
उत्तर- चुनाव घोषणा पत्र एक दस्तावेज है जिसमें उम्मीदवार अपने बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करता है। इसमें शामिल होता है:-
उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले
उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियाँ
शैक्षिक योग्यता
पिछले पाँच वर्षों का आयकर विवरण
सरकारी बकाया, यदि कोई हो
यह घोषणा पत्र मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करता है और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाता है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 16. चुनाव अभियान पर अपना विचार व्यक्त करें।
उत्तर- चुनाव अभियान लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उम्मीदवारों को अपने विचार और नीतियाँ मतदाताओं तक पहुँचाने का अवसर देता है। अभियान के दौरान, उम्मीदवार जनसभाओं, घर-घर जाकर प्रचार, मीडिया विज्ञापनों और सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। हालाँकि, कभी-कभी अभियान में नकारात्मक तत्व जैसे धन का दुरुपयोग या झूठे वादे भी देखे जाते हैं। एक आदर्श चुनाव अभियान मुद्दों पर केंद्रित होना चाहिए और मतदाताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद करना चाहिए।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 17. चुनाव में प्रयोग होनेवाले मशीन का क्या नाम है ? यह कैसे कार्य करता है?
उत्तर- चुनाव में प्रयोग होने वाली मशीन का नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) है। EVM में दो यूनिट होती हैं – कंट्रोल यूनिट और बैलट यूनिट। बैलट यूनिट पर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिह्न होते हैं। मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के बटन को दबाता है। मशीन एक बीप की आवाज करती है और उम्मीदवार का लैंप जलता है। EVM मतों की गणना को तेज और सटीक बनाता है तथा मतपत्रों के दुरुपयोग को रोकता है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 18. मत-पत्र क्या होता है ?
उत्तर- मत-पत्र एक आधिकारिक कागज है जिस पर चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिह्न छपे होते हैं। पारंपरिक मतदान प्रणाली में, मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर लगाता था। मत-पत्र मतदाताओं को अपना वोट गुप्त रूप से डालने की सुविधा देता है। हालांकि, अब अधिकांश चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग किया जाता है, जो मत-पत्र का डिजिटल रूप है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 19. मतदान केन्द्र के चुनाव अधिकारी एवं पीठासीन पदाधिकारी के कार्यों का परिचय दीजिए
उत्तर- मतदान केंद्र के चुनाव अधिकारी और पीठासीन पदाधिकारी के मुख्य कार्य हैं:-
मतदाताओं की पहचान सत्यापित करना
मतदाताओं की अंगुली पर अमिट स्याही लगाना
EVM का संचालन और निगरानी करना
मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करना
मतदान समाप्त होने पर EVM को सील करना
मतदान से संबंधित सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखना
ये अधिकारी निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 20. भारत में चुनाव परिणामों को स्वीकार करने की बाध्यता है । क्यों ?
उत्तर- भारत में चुनाव परिणामों को स्वीकार करने की बाध्यता इन कारणों से है:-
लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार: यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का पालन है।
संवैधानिक प्रावधान: संविधान में चुनाव प्रक्रिया और परिणामों की वैधता स्थापित की गई है।
निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया: स्वतंत्र चुनाव आयोग की निगरानी में निष्पक्ष चुनाव होते हैं।
पारदर्शिता: मीडिया और पर्यवेक्षकों की उपस्थिति पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
राजनीतिक स्थिरता: परिणामों को स्वीकार करना राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 21. ‘री-पोलिंग’ किसे कहते हैं ?
उत्तर- री-पोलिंग’ या पुनर्मतदान तब होता है जब किसी मतदान केंद्र या पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है। चुनाव आयोग पुख्ता प्रमाणों के आधार पर री-पोलिंग का आदेश देता है। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता और शुद्धता सुनिश्चित करना है। री-पोलिंग में केवल प्रभावित क्षेत्र के मतदाता ही भाग लेते हैं। यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 22. भारतीय चुनाव में भागीदारी पर एक टिप्पणी लिखें।
उत्तर- भारतीय चुनावों में मतदान की भागीदारी उत्साहजनक रही है:-
स्थिर या बढ़ता मतदान प्रतिशत: पिछले कुछ दशकों में मतदान प्रतिशत स्थिर रहा है या बढ़ा है।
विविध भागीदारी: गरीब, निरक्षर और कमजोर वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में मतदान करते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च भागीदारी: ग्रामीण इलाकों में मतदान प्रतिशत अक्सर शहरी क्षेत्रों से अधिक होता है।
महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या: हाल के वर्षों में महिला मतदाताओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है।
युवा मतदाताओं का योगदान: नए मतदाताओं की बड़ी संख्या चुनावों में भाग लेती है।
यह व्यापक भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 23. उप चुनाव क्या है ?
उत्तर- उप चुनाव एक विशेष चुनाव है जो निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है:-
सदस्य की मृत्यु होने पर
सदस्य के इस्तीफा देने पर
सदस्य की अयोग्यता घोषित होने पर
सदस्य के निर्वाचन को रद्द किए जाने पर
उप चुनाव केवल एक निर्वाचन क्षेत्र तक सीमित होता है और शेष कार्यकाल के लिए नया प्रतिनिधि चुना जाता है। यह सदन की पूर्ण सदस्य संख्या बनाए रखने के लिए आवश्यक है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 24. मध्यावधि चुनाव क्या है ?
उत्तर- मध्यावधि चुनाव तब होता है जब:-
सरकार अल्पमत में आ जाती है और विश्वास मत हार जाती है
गठबंधन सरकार टूट जाती है
कोई दल या गठबंधन बहुमत खो देता है
प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सदन को भंग करने की सिफारिश करते हैं
मध्यावधि चुनाव में पूरे देश या राज्य में नए सिरे से चुनाव कराए जाते हैं। यह आम चुनाव की तरह ही होता है, लेकिन नियमित पांच साल के कार्यकाल से पहले होता है। इसका उद्देश्य नई सरकार का गठन करना होता है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
Bihar Board class 9 Political Science chapter 4 – दीर्घ उत्तरीय प्रश्न
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 1. चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हैं ?
उत्तर- लोकतांत्रिक चुनावों के लिए कुछ आवश्यक मानदंड होते हैं जो उन्हें वास्तव में जनता के प्रतिनिधित्व का माध्यम बनाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सार्वभौमिक मताधिकार, जहाँ प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का समान अधिकार मिलता है। चुनाव नियमित अंतराल पर होने चाहिए ताकि जनता को अपने प्रतिनिधियों को बदलने का मौका मिले। निष्पक्षता और पारदर्शिता चुनाव प्रक्रिया के आधार स्तंभ हैं, जिन्हें स्वतंत्र चुनाव आयोग सुनिश्चित करता है। बहुदलीय प्रणाली मतदाताओं को विभिन्न विकल्प प्रदान करती है, जिससे वे अपनी पसंद के अनुसार चुन सकें। भारत में इन सभी मानदंडों का पालन किया जाता है, जो इसके चुनावों को लोकतांत्रिक बनाता है। हालाँकि, चुनौतियाँ मौजूद हैं, लेकिन निरंतर सुधारों के प्रयास इन चुनावों को और अधिक मजबूत बनाते हैं।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 2. राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्या अर्थ है ?
उत्तर- राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र का एक आवश्यक तत्व है जो शासन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। यह विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के बीच सत्ता प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ प्रतियोगिता है। इस प्रक्रिया में, प्रत्येक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के सामने रखता है, ताकि उनका समर्थन प्राप्त कर सके। चुनाव प्रचार और अभियान के माध्यम से, वे मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा नेताओं और दलों को जनहित के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और उनके समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करती है। इससे न केवल नए विचारों और नेतृत्व के उभरने का अवसर मिलता है, बल्कि यह जनता को अपने प्रतिनिधियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का मौका भी देता है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 3. भारत में चुनाव कितना लोकतांत्रिक है ? स्पष्ट करें।
उत्तर- भारत में चुनाव प्रक्रिया काफी हद तक लोकतांत्रिक है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। सकारात्मक पहलुओं में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नियमित चुनाव, स्वतंत्र चुनाव आयोग, और बहुदलीय प्रणाली शामिल हैं, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हैं। हालाँकि, कुछ चुनौतियाँ भी हैं जैसे मतदाता सूची में गड़बड़ी, मतदाताओं पर दबाव, सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग, और जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं को प्रभावित करना। इन समस्याओं से निपटने के लिए, भारत ने कई सुधार किए हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग, मतदाता जागरूकता अभियान, और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन। यद्यपि चुनौतियाँ मौजूद हैं, भारत की चुनाव प्रक्रिया लगातार सुधार की ओर अग्रसर है, जो इसे और अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने का प्रयास करती है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 4. चुनाव आयोग के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें।
उत्तर- भारतीय निर्वाचन आयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। इसके प्रमुख कार्यों में मतदाता सूचियों का निर्माण और अद्यतन, चुनाव कार्यक्रम की घोषणा और संचालन शामिल हैं। आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है और उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया का निरीक्षण करता है। यह आदर्श आचार संहिता लागू करता है और मतदान केंद्रों की स्थापना व प्रबंधन करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग, मतगणना प्रक्रिया का संचालन और परिणामों की घोषणा भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साथ ही, यह चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करता है और चुनाव सुधारों के लिए सिफारिशें देता है। इन कार्यों के माध्यम से, चुनाव आयोग भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती सुनिश्चित करता है।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 5. निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान सभा के गठन (2005 ई.) की क्या अधिसूचना जारी की थी?
उत्तर- 2005 में बिहार विधान सभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कई महत्वपूर्ण अधिसूचनाएँ जारी कीं। इनमें मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र को अनिवार्य करना और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना शामिल था। आयोग ने चुनाव खर्च पर सख्त नियंत्रण लागू किया और राजनीतिक विज्ञापनों पर निगरानी बढ़ाई। गुप्त चुनावी खर्च पर विशेष नज़र रखी गई और अपराधी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाने के उपाय किए गए। चुनाव के दौरान कुछ जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया गया। इन उपायों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना था, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति
प्रश्न 6. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग को कौन-कौन से उचित कदम उठाने चाहिए?
उत्तर- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को कई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले, ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारियों की नियुक्ति करना और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से कार्यान्वयन करना आवश्यक है। मतदाता सूचियों की सटीक तैयारी और नियमित अद्यतन के साथ-साथ मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता बनाए रखना और मतदाता जागरूकता अभियान चलाना भी महत्वपूर्ण है। चुनाव खर्च पर प्रभावी नियंत्रण, मीडिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करना, और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना भी आवश्यक है। इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया में नवीन तकनीकों का उपयोग करके इसे और अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है। इन उपायों से चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा।
Bihar Board Class 9 Political Science Chapter 4 Solutions – चुनावी राजनीति